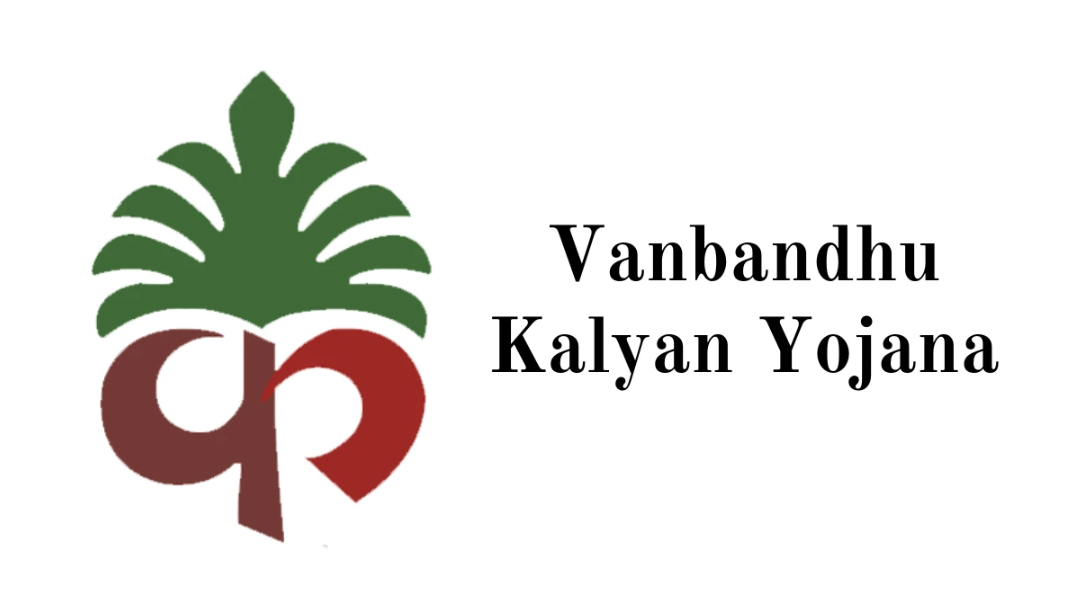परिचय
भारत के आदिवासी समुदायों का देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि, दशकों से आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका के अवसरों की कमी देखी गई है। इसी असमानता को दूर करने और आदिवासियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2014 में “वनबंधु कल्याण योजना” की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है।
वनबंधु कल्याण योजना का उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य
- आदिवासी लोगों के समग्र विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना जैसे – सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा आदि।
- शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना।
- आदिवासी समाज को सांस्कृतिक और सामाजिक संरक्षण देना।
- विभिन्न योजनाओं को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ लागू करना।
योजना की शुरुआत और पृष्ठभूमि
वनबंधु कल्याण योजना को वर्ष 2014 में जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) द्वारा प्रारंभ किया गया। यह योजना तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम की पहल पर बनी थी। योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 राज्यों के 10 जिलों में लागू किया गया और बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया गया।
योजना के प्रमुख घटक
1. बुनियादी ढांचे का विकास
- ग्रामीण सड़कों, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों की स्थापना।
- आश्रम स्कूल और छात्रावासों का निर्माण।
- सामुदायिक भवन और आवास सुविधा।
2. शिक्षा में सुधार
- आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था।
- आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती।
- छात्रवृत्ति योजनाएं और डिजिटल शिक्षा का विस्तार।
3. स्वास्थ्य सेवाएं
- जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण।
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती।
- कुपोषण उन्मूलन अभियान।
- मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं।
4. आजीविका और कौशल विकास
- आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill Development Training)।
- हस्तशिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प जैसे पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा।
- स्वरोजगार योजनाएं और बैंक लिंकेज।
5. सामाजिक और सांस्कृतिक विकास
- जनजातीय त्योहारों, नृत्यों और परंपराओं को बढ़ावा देना।
- सांस्कृतिक भवनों और संग्रहालयों की स्थापना।
- स्थानीय बोली और परंपरागत ज्ञान का संरक्षण।
योजना का क्रियान्वयन तंत्र
राज्य और जिला स्तरीय सहयोग
- योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- हर जिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम के माध्यम से प्रगति की निगरानी।
अन्य योजनाओं के साथ समन्वय
वनबंधु कल्याण योजना को निम्न योजनाओं से समन्वय कर चलाया जाता है:
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- आयुष्मान भारत
- जल जीवन मिशन
- समग्र शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
वनबंधु कल्याण योजना के लाभ
आदिवासी समुदाय को हुए लाभ
- शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बच्चों की स्कूलों में भागीदारी में वृद्धि हुई है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है।
- स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध हुए हैं।
- महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।
- गांवों में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हुआ है।
आलोचना और चुनौतियाँ
योजना में आने वाली समस्याएं
- दूरस्थ क्षेत्रों में योजना की पहुंच सीमित।
- कुछ स्थानों पर फंड का दुरुपयोग या असमान वितरण।
- शिक्षकों और मेडिकल स्टाफ की कमी।
- संवेदनशील इलाकों में प्रशासनिक कठिनाइयां।
सुझाव और समाधान
- योजनाओं के प्रभावी मॉनिटरिंग तंत्र की आवश्यकता।
- स्थानीय युवाओं को योजना में शामिल करना जिससे रोजगार भी मिले और क्रियान्वयन बेहतर हो।
- जनजातीय नेताओं और समुदायों की भागीदारी बढ़ाना।
- डिजिटल माध्यमों से डाटा ट्रैकिंग और पारदर्शिता लाना।
भविष्य की योजनाएं
भारत सरकार इस योजना के तहत 2025 तक निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है:
- 100% स्कूल जाने योग्य बच्चों की नामांकन दर।
- प्रत्येक आदिवासी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा।
- युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करना।
- जनजातीय क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली और जल आपूर्ति।
निष्कर्ष
वनबंधु कल्याण योजना भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जो देश के आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। यह योजना आदिवासियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, मुख्यधारा से जुड़ने और अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का अवसर प्रदान करती है।